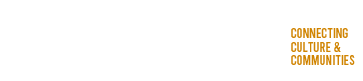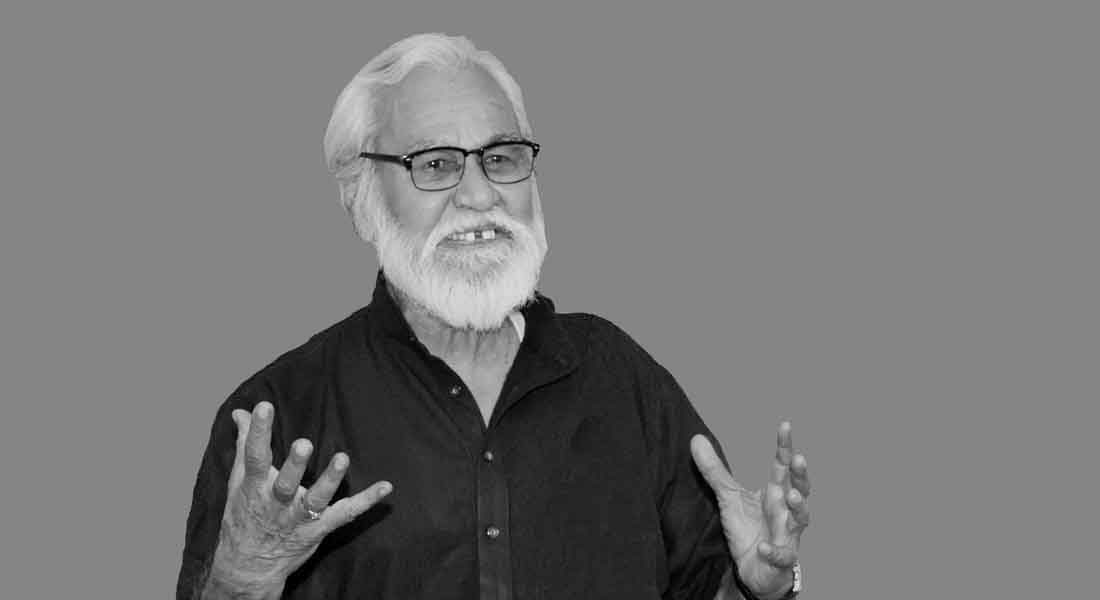लोककलाएं देश की सांस्कृतिक विरासत होती हैं। समाज से इनका गहरा रिश्ता है, इसलिए इनका समाजशास्त्रीय महत्व भी है। यह कहना कठिन है कि इनके प्रणेता कौन थे। लोककलाओं की परंपरा तो ढूंढी जा सकती है, परंतु इनका इतिहास निर्धारित करना कठिन है। दृश्य कलाओं में सबसे प्राचीन लोकचित्र परंपरा है। सामाजिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लोककलाएं पीढ़ी-दर-पीढ़ी संस्कारों की तरह हस्तांतरित होती हैं। समय, परिस्थितियों के कारण ये रूप बदल लेती हैं पर इनका रिश्ता समाज के साथ अक्षुण्ण है।
लोककलाएं अपनी सहजता, सरलता के कारण स्वत: मन की गहराइयों में प्रवेश कर हमारी संवेदनाओं को झंकृत करती हैं। युगों से प्रवाहित लोकसंस्कृति की धारा लोकमंगल की प्रवाहमान परम्परा है। लोकपरंपराएं अपने कालजयी अनुभवों को अपने में समेटकर चलती हैं। पुराने अप्रासंगिक अनुपयोगी संदर्भों को तिलांजलि देकर नये को जोड़ती हुई, परिष्कृत रूप में आगे बढ़ती हैं। जब तक कोई संरचना व्यक्ति की पहचान बनी रहती है, वह उसकी निजी संपत्ति है। जब लोक उसे अंगीकार कर ले, परम्परा उसे आगे बढ़ाए, रचनाकार की पहचान समाप्त हो जाये, लोक उसे घर-आंगन, उत्सव, त्योहारों का अंग मान ले, तब वह लोककला का रूप ग्रहण करती है। सामूहिकता का भाव ही लोककला और संस्कृति का आधार है।
हमारे देश में लोककला की परम्परा अति प्राचीन है और यही हमारी समसामयिक कला की सशक्त आधारशिला भी है। मानव अपनी वाणी से भावनाओं से अभिव्यक्ति करता है, परंतु इससे पूर्व भी वह आकृतियों के माध्यम से अपनी बात कहता रहा है। सामाजिक अभिव्यक्ति ही कालांतर में लोककला के रूप में विकसित हुई। लोकरंजन और लोकमंगल की कामना इसका मूल है। लौकिक वातावरण को अलौकिक बनाने की इसमें अदम्य क्षमता है। लोकजीवन की समरसता ही आज के संस्कारविहीन होते समाज को जोड़ने में सक्षम है। लोककलाएं एक ओर मनुष्य की सृजन प्रतिभा के प्रस्फुटन और विकास का अवसर देती हैं तो दूसरी ओर सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करने का दायित्व भी निभाती हैं।
सामाजिक संस्कृति का लक्ष्य है अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान करना। भारत की विशाल समृद्ध संस्कृति के कारण ही भारत की विशिष्ट पहचान रही है। आज भूमंडलीकरण के कारण हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर हम अपनी संस्कृति से भी विमुख होते जा रहे हैं। यही सामाजिक मूल्यों के पतन का कारण है।
लोककलाएं मानव सभ्यता के विकास-क्रम का जीवन्त दस्तावेज हैं। ये सामाजिक संदर्भों को जोड़ती हैं। किसी देश की लोककलाएं उसके चिंतन, दर्शन और साहित्य का सारतत्व होती हैं। यह ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो कल्पवृक्ष की तरह जीवन की निरन्तरता का संदेश देती है। लोककलाएं हमारी आदिम संस्कृति की निरन्तरता का प्रमाण हैं और प्रासंगिकता का नाम भी है। लोककलाएं बिना किसी बहस या परिचर्चा के निरन्तर अपनी अभिव्यक्ति करती रहती हैं। यही इनके निरन्तर प्रवाह का मुख्य कारण है। लोकसंस्कृति हमारे आचरण को संभालती रहती है और इसी के माध्यम से हम अपने अतीत में जीते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक दृष्टि बनाए रखने में लोककालएं सर्वोत्तम साधन हैं।
लोककलाओं में स्थानीय उपलब्ध रंगों का प्रयोग होता है जिसमें स्थानीय संस्कृति की सहजता दिखाई देती है। रंगों की अलग-अलग छटा का आभास चित्रों में मिलता है। लोककला और लोकसाहित्य में समाज की जो अवधारण है, वह आदमी को आदमी से जोड़ने की क्रिया है। समातन संबंधों की तलाश है। समाज के ठहराव को गति देने का प्रयास है और जड़ मान्यताओं के परिवर्तन का संकल्प भी।
लोककला का आनंद लेने के लिए सतही दृष्टि नहीं चाहिए, ऐसी दृष्टि की आवश्यकता है जो उसके भीतर के सौदर्य को देख सके। आज व्यावसायिकता में लोककला के मूल तत्व बिखर रहे हैं, सहजता, सरलता नष्ट हो रही है। लोककला का मूलरूप खोता जा रहा है। कला में परिवर्तन ग्राह्य है पर उच्छृंखलता का कोई स्थान नहीं है। लोककला के व्यावसायीकरण के कारण, ग्राहकों को तुष्ट करने के लिए या प्रयोगों के नाम पर लोककला के मूलरूपों में अमूल परिवर्तन से लोककला को बड़ा खतरा है। समाज को कला का आनंद लेने के लिए कला सौंदर्यबोध को जगाना होगा। उन्हीं लोक-कृतियों का चयन करना होगा जिनमें लोकतत्व निहित हैं।
विद्वानों के अनुसार लोककलाओं के अनेक रूप हैं जिनमें प्रमुख हैं – लोककला, लोकशिल्प, लोककथाएं, लोकनाट्य, लोकसंगीत, लोकनृत्य, लोकव्यवसाय आदि। इनमें लोक अर्थात् जनसामान्य की मुख्य भूमिका है। इसमें प्रचलित प्रतीकों का प्रयोग होता है जो मुख्यत: बिन्दु, ओंकार, स्वास्तिक, लहर, रेखा, त्रिकोण (ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी), सप्तमात्रिका, षोड्शमात्रिका, दशावतार, शुभ पशु-पक्षी, चौक, थापा, कोहबर, वेदी, कलश, आरती, वन्दनवार, मेंहदी, महावर, गोदना आदि। प्राकृतिक प्रतीकों में सूर्य, चंद्र, कमल, बांस, कछुआ, दही-मछली, पंखा, पुरइन, गाय, केला वृक्ष, पीपल वृक्ष, नदी, पर्वत, आदि।
लोककलाओं की समग्र दृष्टि व्यक्ति के लिए नहीं, समष्टि के लिए होती है जो सहज जीवन की प्रेरणा देती है। हमारे मन-मस्तिष्क में रस का संचार करती है, जीवन को आनन्दमय बनाती है। दुख व्यक्ति अकेले झेल लेता है पर आनन्द सब के साथ मनाना चाहता है। लोककलाओं का उद्देश्य ही रस की प्राप्ति है। आज आदमी व्यक्ति रूप में भी पूर्णता का बोध नहीं कर पाता। विभिन्न जातीय कारीगरी के नमूने भी लोककलाएं हैं, जो पिता अपने पुत्र को सिखाता है, मां अपनी बेटी को सिखाती है। यह भावना ही सृष्टि-चक्र का नियामक है। इसी के द्वारा कला में जीवन मूल्य सुरक्षित रहते हैं। समाज सौंदर्यबोध की दीक्षा पाता है।
लोककलाओं की विशेषता है कि ये अपने मूल स्वरूप की ओर जाते हुए भी नई ऊर्जा, नए परिवर्तन ग्रहण करती रहती है। इनके दर्शन से तनावों की मुक्ति मिलती है। हास-परिहास भी लोककला का अंग है। यहां कुण्ठाओं, वर्जनाओं का कोई स्थान नहीं है। लोकलाएं आदि मानव की आवश्यकताएं थीं और आज भी उन्हें देखकर विश्वास होता है कि आज भी आदमी अपने भीतर आदिम रूप में जी रहा है। सहज आवरणहीन जीवन। लोककला की सहजता, पूर्णता का आभास पाकर वह संतोष पाता है।
आज सांस्कृतिक अवमूल्यन के संकट-काल में लोककलाओं के अध्ययन से भारतीय संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा होगी। आस्थावान लोगों को पुनर्विश्वास मिलेगा और उपेक्षा करने वालों को खोये हुए निजत्व को वापस पाने का आमंत्रण। आज आवश्यकता है अपने देश की उत्सवप्रियता को अपनाने का लोककला और शिल्पों की महत्ता को पहचानने का, उन्हें जीवन में समुचित स्थान और आदर देने का।
—
Read more
पद्मश्री प्रोफेसर श्याम शर्मा: एक संस्मरण, लखनऊ-1966
कला संवादों से निखरती है हमारी कला: पद्मश्री प्रो. श्याम शर्मा
कला नितांत ही व्यक्तिगत साधना है: पद्मश्री श्याम शर्मा
Reference
पद्मश्री श्याम शर्मा की पुस्तक ‘कला और शिल्प ‘ से साभार
—
Disclaimer: The opinions expressed within this article or in any link are the personal opinions of the author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Folkartopedia and Folkartopedia does not assume any responsibility or liability for the same.
Folkartopedia welcomes your support, suggestions and feedback.
If you find any factual mistake, please report to us with a genuine correction. Thank you.