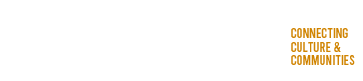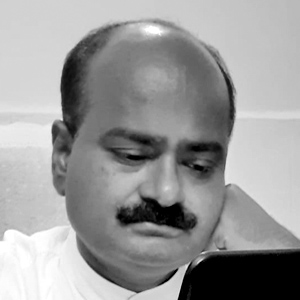
आचार्य कैलाश कुमार मिश्र, संस्थापक-चेयरमैन-सीईओ, ब्रेनकोठी । वरिष्ठ कला समालोचक (लोककला) एवं ख्यातिलब्ध संस्कृतिकर्मी ।
—
ताम्र एक औषधीय धातु है। आयुर्वेद में और सघन जनजातीय क्षेत्रों में लोग ताम्र का प्रयोग अनेक रोगों के उपचार के लिए करते हैं। इसका प्रयोग लोहे के ज्ञान होने से बहुत पहले से होता रहा है। ताम्र विद्युत् का सुचालक और अग्नि तत्व से भरपूर है। भारतीय सनातनी हिन्दू परंपरा में उत्सव, अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना में ताम्र-पात्रों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। वराह पुराण में ताम्र से संबंधित एक रोचक प्रसंग मिलता है।
उस प्रसंग के अनुसार गुडाकेश नामक एक दैत्य था जो विष्णु का परम भक्त था। एकबार गुडाकेश हठयोगी बनकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट होते हुए बोले: “मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें”। गुडाकेश बोला: “हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दें कि आपके चक्र से मेरी मृत्यु हो और मृत्यु के तुरंत बाद मेरा शरीर ताम्र में परिवर्तित हो जाए और उसका उपयोग आपकी पूजा के लिए बनाने वाले पात्रों में हो। ऐसी पूजा से आप प्रसन्न हों। इससे ताम्र पवित्र धातु बन जाएगा”। भगवान विष्णु ने गुडाकेश को तथास्तु कहा और समय आने पर चक्र से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। गुडाकेश के मांस से ताम्र, रक्त से सोना और अस्थियों से चांदी का निर्माण हुआ।
अब वाराणसी की ताम्र-कला पर आते हैं। पूजा के लिए पवित्र समझे जाने के कारण जितने भी भक्त वाराणसी तीर्थक्षेत्र में आते हैं, वे सभी ताम्र-पात्र में गंगाजल, फुलडाला एवं अनेक वास्तु खरीदते हैं। वहां ताम्र-पात्र की परंपरा एक पुरातन उद्योग के रूप में है। उस उद्योग का स्वरूप पिछले पचास वर्षों में क्या रहा है, सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं।
ताम्र-कला (उद्योग) का सार्वभौमिक स्वरूप
घर्मनगरी वाराणसी में पीतल एवं ताम्बे से बने कलात्मक वस्तुओं एवं पात्रों का प्रचलन अन्य उद्योग जैसे साड़ी तथा काष्ठ-कला के समान ही अति प्राचीन है। इसका मुख्य कारण काशी का पुण्यधाम होना है। जब तीर्थयात्री बनारस आते थे तो वे लोग वहां विभिन्न तरह के संस्कार तथा पूजा-पाठ में उपयुक्त होने वाले पात्रों को खरीदते थे। कुछ पात्र खरीदकर घर भी ले जाते थे। इन्हीं कारणों से यह उद्योग विकसित तथा पुष्पित होता रहा है। यहां के पात्रों की कलात्मकता इतनी अच्छी है कि इनकी मांग धीरे-धीरे अन्य धार्मिक स्थानों एवं नगरों में भी होने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब वाराणसी में बनने वाले पात्रों एवं वस्तुओं, खासकर अनुष्ठान से जुड़ी वस्तुओं यथा सिहांसन, त्रिशूल, घंटी, घंटा, घुंघरु आदि की मांग देवघर, वृन्दावन, उज्जैन से लेकर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर तक होने लगी। इसके साथ-ही-साथ ताम्र-कलाकारों ने सजावटी वस्तुओं, घरेलू पात्र, मूर्तियां, एन्टीक पीस एवं अन्य कलात्मक उत्पाद बनाने प्रारंभ कर दिये जिनकी मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती गयी।
प्रारंभ में वाराणसी में केवल धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाले पात्रों का निर्माण होता था जिनके नाम इस प्रकार है:
- पंचपात्र
- अघ्र्य
- आचमन
- दीप
- फूलों की डलिया (फूल डाली)
- घंटी
- घंटा
- मंगल कलश
- त्रिशूल
- लोटा
- कमण्डल
- मूर्ति
- झालर
- घुंघरु आदि।
मुसलमानों के भारत आगमन के बाद ताम्र उद्योग (कला) पर भी इस्लाम का प्रभाव पड़ा और इस्लाम की कला भी उससे प्रभावित हुई। धीरे-धीरे यहां के ताम्र-कलाकारों ने मुसलमानों के शादी-विवाह या अन्य उत्सवों में प्रयुक्त होनेवाले नक्काशीयुक्त बर्तन (पात्र), थाल, तरवाना इत्यादि बनाना प्रारंभ किया। पात्रों की कलात्मकता में अत्याधिक आकर्षण था, लिहाजा उसके आकर्षण से हिन्दू भी अप्रभावित नहीं रह सके। धीरे-धीरे हिन्दुओं ने भी उन पात्रों का उपयोग उत्सवों तथा शादी-विवाह आदि के आयोजनों में करना प्रारम्भ कर दिया।
कालांतर में मुसलमानों द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले ‘बदना’ का निर्माण भी कलात्मक ढंग से काशी के कसेरों ने प्रारंभ किया। ‘बदना’ में इनके द्वारा निखारी गयी कलात्मकता ने संभ्रान्त मुसलमानों, यहां तक कि मुगल बादशाहों, रईसों और लखनऊ के नवाबों का भी मन मोहा। उनकी कला-क्षमता तथा प्रयोगवाधर्मिता से प्रभावित होकर उन्होंने काशी के ताम्र-कलाकारों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। प्रोत्साहन आर्थिक मदद तथा सामाजिक मर्यादा या सम्मान दोनों ही रूप में दिया जाता था। ताम्र-कलाकारों ने भी इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप अनेक प्रयोग किये, जिससे उनकी कृतियों में और निखार आया। इस तरह पारंपरिक वस्तुओं और हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ-साथ वाराणसी के ताम्र-कलाकारों ने कलात्मक उत्पादों का निर्माण जारी रखा।
स्टील तथा अल्यूमिनियम से उपजा संकट और उसका समाधान
सत्तर तथा अस्सी के दशक में बाजार में एकाएक स्टील तथा अल्यूमिनियम का धमाके के साथ आगमन हुआ। जहां ताम्बे, पीतल, कांसे के पात्रों की कीमत दिन प्रतिदिन चढ़ रही थी, वहीं स्टील के बर्तन काफी सस्ते थे। स्टील और अल्यूमिनियम के बर्तनों का निर्माण बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में किया जाता रहा था। अत: स्वाभाविक रूप से उसमें मजदूरी भी काफी कम लगती थी। कुछ ही वर्षों में अल्यूमिनियम और स्टील के उत्पादों ने बाजार पर कब्जा कर लिया। स्टील की वस्तुएं ‘आइडेन्टीटी प्राइड’ बन गयीं। थाली, रसोई के बर्तन, ग्लास, कप के साथ-साथ पूजा के थाल, फूलों की डलिया, कमंण्डल इत्यादि जैसे चीजों का भी निर्माण स्टील से होने लगा। हालांकि यज्ञ-अनुष्ठानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन को अपवित्र माना गया है, परन्तु पण्डितों एवं शास्त्रज्ञों ने बहुत से अनुष्ठानिक क्रिया-कलापों में भी स्टील के पात्र को व्यवहार में लाने की इजाज़त दे दी। धीरे-धीरे स्थिति इतनी विकट हो गई कि काशी के विश्वनाथ गली में ताम्रपात्र तथा अन्य कलाकृति बेचने वाले व्यवसायी ताम्र-पात्र कम और स्टील पात्र अधिक बेचने लगे।
इन परिस्थितियों में ताम्र-कलाकारों ने धैर्य से काम लिया। उन्होंने अपना ध्यान डिजाइन को आकर्षक बनाने, एनटीक पीस बनाने, शो-पीस, गुलदस्ते, फूलों का गुच्छा, किंरग, बच्चों के खिलौने, सजावटी वस्तुएं बनाने, लेम्प, वॉल हैंगिंग, काशी के विश्वनाथ मंदिर और विभिन्न घाटों की नक्काशी, गंगा नदी, देवी-देवताओं की प्लेट पर नक्काशी इत्यादि बनाने में केंद्रित किया। इससे निर्माण की प्रक्रिया मंद जरूर हुई, परन्तु ताम्र कला का अन्त नहीं हुआ। धीरे-धीरे जब धर्मनगरी वाराणसी की ख्याति तथा सारनाथ के ऐतिहासिक महत्त्व से प्रभावित होकर वहां तीर्थयात्रियों, धर्मार्थियों के साथ-साथ देशी तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या वहां बढ़ी, तब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताम्र-कलाकारों ने सारनाथ के सभी ऐतिहासिक दृश्य, महाप्राण भगवान गौतम बुद्ध, महावीर, महाराजा अशोक, अशोक स्तंम्भ के मुखों वाला सिंह, गंगा घाट इत्यादि की कलात्मकत वस्तुओं को कलात्मक ढंग से गढ़ना शुरू किया। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के चित्रों को ताम्र में गढ़ना प्रारंभ किया। आज इन कलात्मक वस्तुओं की बाजार में अच्छी मांग है और इससे उन्हें आमदनी भी अच्छी हो जाती है।
वाराणसी में ताम्र कला का एक सच यह भी है कि गत पचास वर्षों में विभिन्न कारणों से ‘मेटल वर्करो’ की संख्या में कमी आयी है। यह एक आश्चर्यजनक बात है। एक ओर जहां सिल्क साड़ी तथा वस्त्र उद्योग एवं काष्ठ-कला के शिल्पकारों की संख्या में लगातार बृद्धि हो रही है, दूसरी ओर ताम्र तथा अन्य मेटल उद्योग में लगे शिल्पकारों की संख्या में दिन-प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। निश्चित ही यह एक विचारणीय प्रश्न है।
ताम्र-कलाकारों का वर्गीकरण
वाराणसी के ताम्र-कलाकारों को मोटे तौर पर चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- रिपोजी या इन्ग्रेविंग करने वाले कलाकार
- धार्मिक अनुष्ठान में प्रयुक्त पात्रों का निर्माण करने वाले कलाकार
- सजावटी समान (एन्टीक पीस) इत्यादि का निर्माण करने वाले कलाकार और
- धरेलू बर्तनों का निर्माण करने वाले कलाकार।
ताम्र-कलाकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो पुराने ताम्बे के पात्रों को गलाने का काम करता है। वे ताम्बे को गलाकर उसके केक को पिटउआ बर्तन या पात्र बनाने के लिए ताम्र-कलाकारों को दे देते हैं।
रिपोजी करने वालों की संख्या तेजी से घटी है। आज मुश्किल से 15 परिवार इस पेशे में हैं। रिपोजी करने वाले लोग पहले बड़े-बड़े रईसों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले आराम तथा डेकोरेशन की चीजों यथा कुर्सी, पलंग, इत्यादि में नक्काशी या रिपोजी का काम करते थे। इसके अलावा मंदिरों के गुम्बद, मस्जिद की मीनार, राजमहलों एवं रईसों की हवेलियों के छत पर भी रिपोजी का काम धातुओं जैसे चांदी, सिल्वर या अन्य चमकदार धातुओं से किया करते थे। हालांकि फर्नीचर पर रिपोजिंग कराने की प्रथा का लगभग अन्त-सा हो चुका है, परन्तु मंदिरों इत्यादि के लिए आज भी इन्हें भारत के विभिन्न प्रांतों से बुलाया जाता है। कुछ लोग तो नेपाल और श्रीलंका तक जाते हैं।
कुछ ताम्रकार या ताम्र-कलाकार धार्मिक अनुष्ठान में प्रयुक्त होनेवाले बर्तनों के निर्माण में लगे हुए हैं। इन्हें भी मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है:
- वे जो धातुओं को पीट-पीटकर सामान या पात्र बनाते हैं,
- वे जो ढलाई के बाद मशीन पर बर्तन अथवा पात्र को गढ़ लेते हैं।
वाराणसी में ताम्र-कलाकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो एन्टीक पीस और अन्य कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लगा है। इनकी सोच की सीमा असीम है। अपनी कलाकृतियों में चाहे गंगा नदी, बनारस के घाट, विश्वनाथ मंदिर, भगवान गौतम बुद्ध की आकृति, सारनाथ के ऐतिहासिक अवशेषों का चित्रण कुछ भी क्यों न हो, ये कलाकार बखूबी उसकी इनग्रेविंग करते हैं।
अंतिम समूह घरेलू समान जैसे रसोई में प्रयुक्त होने वाले पात्र यथा – लोटा, बदना, कड़ाही, कलछुल, ग्लास इत्यादि के निर्माण में लगे हैं। शादी तथा विवाह के अवसरों पर प्रयुक्त मंगल-कलश, प्रतिभोज इत्यादि में प्रयुक्त भोजन के बर्तन इत्यादि का निर्माण भी इन्हीं कलाकारों द्वारा किया जाता है। इनके अलावा ढलाई के द्वारा जो समान बनाये जाते हैं, उसमें आजकल सेवई बनाने की मशीन इत्यादि को भी बनाने का काम बहुत से कलाकार कर रहे हैं।

प्रमुख ताम्र-कलाकृतियों के नाम
- लोटा
- कमण्डल
- फूलों की डलिया
- गंगा जल पात्र
- वरगुणा
- अघ्र्य/अरघा
- पंचपात्र
- घुंघरु
- बदना
- पानदान
- घंटी
- देवी-देवताओं की मूर्तियां
- एन्टीक पीस
- मंगल कलश
- झूले
- पालना
- तबला
- झालर
- रसोई में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पात्र
- घण्टी
- तरबाना/कोपर (कन्या दान के समय प्रयुक्त किया जानेवाला पात्र।)
- आचमनी।
ताम्र-कलाकारों की आर्थिक स्थिति
अगर वाराणसी के ताम्र-कलाकारों की आर्थिक स्थिति की तुलना काष्ठ तथा वस्र उद्योग में लगे हस्त शिल्पियों से करें, तो इन्हें कमजोर कहा जा सकता है। काशीपुरा के श्रीराम जो पीतल को पीट-पीट कर तबला तथा बांया बनाते हैं, उनके मुताबिक वे एक दिन में 3 किलो तक पीतल की पिटाई कर देते हैं। इसके लिए इन्हें मेहनताना वजन के हिसाब से दिया जाता है। एक किलो पीतल की पिटाई पर 20 रुपये मेहनताना मिलता है, अर्थात् एक कारीगर प्रतिदिन 40 रु. से 60 रु. तक कमाता है।
इसी तरह से मेहनताना उन लोगों को भी दिया जाता है जो तांबा गलाने का काम करते हैं। इस काम में लगे श्रीनाथ के अनुसार उन्हें 1.50 रु/किलो के हिसाब से मजदूरी दी जाती है और बिजली की सप्लाई सही रही, तब 12 घंटे में 3 आदमी मिलकर करीब 2 क्विंटल माल गला देते हैं। यानी, प्रति व्यक्ति 100 रुपये की कमाई होती है। लेकिन उन्हें यह भी नसीब नहीं है क्योंकि बिजली कुछ घंटे ही उपलब्ध हो पाती है।
सिल्वर प्लेट से मशीन द्वारा जो समान बनाते हैं, उन्हें मेहनताना वजन तथा नगवार दोनों हिसाब से दिया जाता है। अगर पात्र बड़ा हो, तो 3 रुपये/किलो और अगर छोटे-छोटे तथा कलात्मक पात्र हों, तो फिर नग। पैसा देने का हिसाब आना होता है। 12 आना, 16 आना, 20 आना आदि के हिसाब (एक आने में 6 पैसा होता है तथा 16 आने का एक रुपया होता है) से पारिश्रमिक दी जाती है। इस दृष्टिकोण से मेहनती कलाकार भी 40 रु. से 60 रु./दिन तक ही कमा पाते हैं।
यह राशि निश्चित रूप से वस्र तथा काष्ठ-कलाकृतियों के व्यवसाय में लगे कलाकारों की तुलना में काफी कम है। संभवतः यही कारण है कि धीरे-धीरे लोग इस व्यवसाय को छोड़ रहे हैं। कुछ ताम्र-कलाकार तो वाराणसी को छोड़कर अन्य जगहों में चले गये हैं जहां इन्हें अधिक मेहनताना तथा सम्मान के साथ-साथ अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वाराणसी के बहुत से ताम्र-कलाकार आजकल तेजी से मिर्जापुर और नेपाल के काठमांडू इत्यादि शहरों में जा रहे हैं।
दूसरा कारण यह है कि ताम्र-पात्रों के प्रति लोगों का रुझान काफी कम है। हालांकि आजकल वह रुझान फिर से पनप रहा है, जिसका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। इनके अलावा अनुष्ठान में प्रयुक्त होनेवाले बहुत से ताम्बे-पीतल के कलात्मक पात्रों एवं कलाकृतियों को वाराणसी से काठमांडू भेजा जाता था। मांग अच्छी होने के कारण इन्हें पारिश्रमिक भी अधिक मिलती थी। आजकल कस्टम ड्यूटी बढ़ने के कारण उन उत्पादों की कीमतें काफी बढ़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप लोग बढ़ी हुई कीमत पर अच्छी कलात्मकता वस्तुओं को भी नहीं खरीदना चाहते हैं।
निष्कर्ष यह कि वाराणसी के कारीगर बहुत बड़ी तादाद में इस धंधे को छोड़कर अन्य धन्धों को अपनाना रहे हैं और बहुत से कारीगरों का पलायन नेपाल, मिर्जापुर एवं अन्य जगहों पर हो रहा है। यह एक दुखद स्थिति है।
ताम्र-कलाकारों की समस्या एवं उनके द्वारा बताए गये समाधान
वाराणसी के ताम्र-कलाकारों के समक्ष यों तो अनेक समस्याएं हैं परन्तु उन सभी समस्याओं में कच्चे माल की कमी एक विकट समस्या है। कुछ व्यापारी थोक के भाव कच्चा माल खरीदकर इन मेहनतकश लोगों का शोषण करते हैं। कच्चा माल दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है:
- सरकार से नीलामी के द्वारा तथा
- कबाड़ी के माध्यम से।
वाराणसी के ताम्र-कलाकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत विभाग, टेलीफ़ोन (डाकतार विभाग) विभाग एवं अन्य विभागों में व्यवहार किए हुए ताम्बे एवं पीतल के तार एवं अन्य चीजों की नीलामी की जाती है। नीलामी थोक भाव से होती है। इसमें सामान्य एवं गरीब तबके के ताम्र-कलाकार चाहकर भी भाग नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास थोक में माल खरीदने का सामर्थ्य नहीं होता। उनकी इसी विवशता का फायदा बड़े व्यापारी उठाते हैं। ये व्यापारी थोक भाव में माल खरीदकर उसका भण्डारन कर लेते हैं और फिर मनमाने मुनाफे पर कच्चा माल बेचते हैं। कुछ व्यापारी कच्चा माल उन्हीं ताम्र-कलाकारों को देते हैं जो अपना तैयार माल उन्हें ही बनाकर दें। इस तरह शोषण चलता रहता है। हालांकि यहां के ताम्र, कांस्य एवं अन्य कला के निर्माण में संलग्न कलाकारों ने ‘अलौह धातु निर्माण कलाकार संगठन” नामक एक संगठन बनाया है, लेकिन संगठन बहुत से कारणों से सही ढंग से काम करने में असफल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार नीलामी न करके पूरे माल संगठन को दे, तब कलाकारों को जरूरत के मुताबिक और वाजिब मूल्य पर कच्चा माल मिल सकता है और इससे उन कलाकारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।
ताम्र-कला में प्रयुक्त उपकरण (औजार)
ताम्र-कला में उपकरण (औजार) की तुलना में हाथ की सफाई तथा मानसिक सोच का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसमें बहुत ही सीमित औजारों का प्रयोग किया जाता है। जो लोग पूर्व में व्यवहार किये गये उपकरणों को खरीदकर उसे गलाते हैं और प्लेट बनाते हैं वे निम्नलिखित औजारों का प्रयोग करते हैं:
- छोटी संख्या (संडसी)
- बड़ी संडसी
- छोटा चिमटा
- बड़ा चिमटा
- कलछुल (बड़े साइज का)
- सब्बल (दो बड़े आकार में)
- घड़ियां (यह ताप का कुचालक होता है। घड़ियां बनारस में नहीं बनाई जाती हैं बल्कि यह चेन्नई से बनकर यहां आती हैं। यह घड़े तथा बाल्टी की आकृति में होती हैं। इसका व्यवहार कच्चे माल को गलाने के लिये किया जाता है। एक पच्चीस न. के घड़िया में, जो विभिन्न नंबरों तथा आकृतियों में उपलब्ध होता है, 40 किलो तक कच्चे माल को पिघलाया जाता है।
- डाई (इसमें गले पिघले हुए माल को डालकर उसका प्लेट बनाया जाता है।)
- हथौड़ा
इसी तरह से पीटकर बनाए जाने वाले पात्रों के निर्माण के लिए निम्नलिखित औजारों को उपयोग में लाया जाता है:
- सबरा
- मधन्ना (मधन्ना एक प्रकार की छोटी हथौड़ी है जिससे पीटा जाता है और उपकरण तैयार किया जाता है।)
- हथौड़ा
मशीन से बनाए जानेवाले पात्रों एवं कलाकृतियों में केवल निम्नलिखित औजारों का प्रयोग हाथ द्वारा यहां के कलाकार करते हैं:
- हवाई स्टील (यह छोटे बड़े विभिन्न आकार में उपलब्ध होता है।)
- डाइमण्ड स्टील (इसका प्रयोग काटने के लिए किया जाता है)।
हवाई स्टील का काम खुरचने तथा आकृति देने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार एन्टीक पीस, बनाने के लिए भी मधन्ना, सबरा, हथौड़ा, प्रकाल, स्केल इत्यादि औजारों की सहायता ली जाती है।
वाराणसी में ताम्र-कलाकारों की लगभग 75 से 80 फीसदी आबादी काशीपुरा मुहल्ले की तंग गलियों में रहती है। मुख्य मार्ग पर बड़े व्यापारियों एवं अन्य दुकानदारों की दुकानें हैं। चूंकि ये लोग शहर में रहकर ही इस धंधे को वर्षों से करते आ रहे हैं, अतः अपनी बढ़ती आबादी के साथ कम-से-कम जगह में ज्यादा-से-ज्यादा लोग रहने पर मजबूर हैं। एक-एक घर में (साइज 30-35 मीटर) चार-चार परिवार के लोग बहुमंजली मकानों में तंगी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। इनके मकान चारों तरफ से बंद है, जहां हवा, रोशनी जाने की कोई व्यवस्था अथवा विकल्प नहीं है। हालांकि आजकल कुछ लोगों ने काशीपुरा की तंग गलियों से निकालकर नई कालोनियों तथा कस्बों में रहना प्रारंभ किया है, परन्तु इनकी संख्या काफी कम है।
—
All Photos Credit: http://www.dsource.in/
—
Other links:
प्रलेखन: बनारस की वस्त्रकला: डॉ. कैलाश कुमार मिश्र
—
Disclaimer: Write-up partially edited. The opinions expressed within this article or in any link are the personal opinions of the author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Folkartopedia and Folkartopedia does not assume any responsibility or liability for the same.
Folkartopedia welcomes your support, suggestions and feedback.
If you find any factual mistake, please report to us with a genuine correction. Thank you.
Tags: Copper art, Copper craft, Copper industry in Varanasi, Dr. Kailash Kumar Mishra, Kailash Mishra