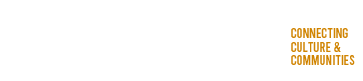सुनील कुमार
कला शोधार्थी, लोक कलाओं के अध्ययन में विशेष रुचि
—
पत्थरकट्टी 1940 के पूर्व बिहार में गौड़ ब्राह्मण शिल्पियों का गढ़ था। अन्य जाति के लोगों की बसावट के बावजूद पाषाण शिल्प का काम सिर्फ गौड़ ब्राह्मण करते थे। शिल्पी हिन्दू देवी-देवताओं के साथ-साथ बुद्ध-महावीर की मूर्तियां भी तराशते थे और दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद भी। 1940 के बाद राजनीतक उथल-पुथल और द्वितीय विश्वयुद्ध के दुष्प्रभावों से पाषाण शिल्पी बुरी तरह प्रभावित हुए। बाजारों में पाषाण शिल्प उत्पादों की मांग न के बराबर रह गयी और उससे उपजी आर्थिक बदहाली ने पाषाण शिल्पियों को जयपुर की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। 1947-48 में गया के जिलाधिकारी जे.सी. माथुर और उपेंद्र महारथी के सहयोग से उन्हें विकट हालात से उबरने में थोड़ी मदद मिली, लेकिन पत्थरकट्टी उस मांग को हासिल नहीं कर पाया जो 1940 से पूर्व बतायी जाती है। एक नजर 1940 से 70 के बीच बन रहे उत्पादों, उनके डिजाइन, आवश्यक स्रोतों और संबंधित उपकरणों पर –
उत्पादों का वर्गीकरण
1970 के दशक के पूर्व पत्थरकट्टी में जिन मूर्तियों एवं प्रस्तर उत्पादों को तराशा जा रहा था, उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: –
धार्मिक उपयोग के उत्पाद
शिल्पकार मुख्य रूप से देवी-देवताओं, बुद्ध और महावीर की मूर्तियां तराशते थे, जिनकी मांग सालो भर थी। उनके अलावा मुख्य रूप से पंचदेवता को बनाया जाता था। द्वितीय विश्वयुद्ध तक पंचदेवता की मूर्तियों की मांग खूब थी क्योंकि उन्हें अमूमन हर गांव में स्थापित करने की परंपरा थी और उनकी उपस्थिति शुभ मानी जाती थी। इन मूर्तियों की ऊंचाई आमतौर पर 5 इंच से 12 इंच तक होती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पंचदेवता की मूर्तियों की मांग घट गयी। आजादी के बाद जब पत्थरकट्टी में ई. डंकन के नेतृत्व में ट्यूशन क्लास शुरू हुई, तब उसमें पंचदेवता को तराशने के लिए युवा शिल्पियों को प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसकी वजह क्या थी, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तब कृष्ण और काली की मूर्तियां भी बनायी जाती थीं।
दैनिक उपयोग के उत्पाद
यह माना जाता है कि 1940 से पूर्व पत्थरकट्टी में बनने वाले घरेलू और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की काफी मांग थी। उनमें पत्थर के कप-प्लेट, थालियां, कटोरे, गिलास, खरल-मूसल, कुंडी, मलिया आदि शामिल थे। 1960-70 के दशक में भी ये उत्पाद पत्थरकट्टी में तराशे जा रहे थे। हालांकि मांग पहले के मुकाबले काफी घट गयी थी क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी थी और उन उत्पादों को बनाने के लिए उपयुक्त पत्थरों को हासिल करने में या उन्हें खदानों से निकालने में अत्यधिक श्रम लगता था। लिहाजा लागत मूल्य ज्यादा था, जबकि सिंहभूम और घाटशिला से आने वाले वे ही उत्पाद ज्यादा सस्ते थे।
दैनिक उपयोग की वस्तुओं में सबसे ज्यादा मांग खरल की थी जिसे किश्तीनुमा या नाव के स्वरूप में बनाया जाता था। खरल का उपयोग औषधियों को पीसने और उन्हें मिलाने के लिए किया जाता था। आमतौर पर इसके साथ एक मूसल या लोढ़ी होती थी। खरल का उपयोग औधषियों या उनके मिश्रण को संभलकर रखने के लिए भी किया जाता था। खरल अलग-अलग आकार के होते थे, 3 इंच से लेकर 24 इंच तक। गोल कटोरेनुमा खरल को कुंडी कहा जाता था जिसका व्यास 5 इंच से 12 इंच तक का होता था। तेल रखने वाला मलिया या छोटा कुंडी 3 इंच का बनाया जाता था।
सजावटी व आनुष्ठानिक उत्पाद
इस श्रेणी में शिव, सरस्वती, सूर्य, बुद्ध, महावीर आदि की छोटी-छोटी मूर्तियां शामिल थीं। बेहद कलात्मक और उच्च कोटि की इन मूर्तियों की मांग पूरे वर्ष रहती थी। पास ही में बोधगया है जहां तब भी बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन संपन्न होते थ। इन आयोजनों की वजह से बौद्ध अनुयायियों का सालो भर वहां आना होता था जिससे बुद्ध मूर्तियों की मांग बनी रहती थी। बुद्ध मूर्तियां 3 इंच से लेकर 18 इंच तक की बनायी जाती थीं जबकि अन्य मूर्तियां 5 इंच से 15 इंच तक की।
उत्पादों के डिजाइन
पत्थरकट्टी में बनने वाली मूर्तियों में पंचदेवता प्रमुख थे जिनमें महादेव, पार्वती, गणेश, नंदी और कृर्तमूर्त को साकार किया जाता था। इनमें महादेव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग को बनाया जाता था जिसके पांच डिजाइन प्रचलित थे और आज भी उनका प्रयोग किया जाता है। वे डिजाइन हैं:
- बांग्ला डिजाइन – इसमें शिवलिंग एक ही पत्थर को काट कर बनाया जाता था, जिसमें शिवलिंग, अर्घ और गौरी (आधार) शामिल होता था। गौरी और अर्घ का निचला हिस्सा मिलने से एक डमरूनुमा डिजाइन बनता था जिसकी वजह से इसे डमरूधर बांग्ला डिजाइन भी कहा जाता था। इसमें एक अन्य डिजाइन भी बनता था जिसे बनारसी बांग्ला डिजाइन कहते थे।
- गौरीपत डिजाइन – इस डिजाइन में गौरी, अर्घ और लिंग को अलग-अलग बनाकर उसे बाद में एक साथ जोड़कर शिवलिंग तैयार किया जाता था। स्थापना के समय इसमें गौरी को गौरी भूमि में दबा दिया जाता था, जबकि अर्घ और लिंग भूमि से ऊपर दिखाई देते थे।
- नागफनी डिजाइन – यह बांग्ला डिजाइन जैसा ही दिखता था, लेकिन इसमें शिवलिंग के ऊपरी हिस्सी में एक सर्पआकृति या नाग बनाया जाता था जो अपना फन फैलाये हुए होता था। इसी वजह से उसे नागफनी डिजाइन भी कहा जाता है।
- नंदी-महादेव डिजाइन – इसमें शिवलिंग को एक ही पत्थर से तराशा जाता है जिसमें नंदी बैल या बसहा को अर्घ के कोनदार हिस्से की तरफ मुंह किये हुए दिखाया जाता है। चूंकि दोनों ही मूर्तियों को एक ही पत्थर से तराशकर बनाया जाता है, इसलिए इस डिजाइन को नंदी-महादेव डिजाइन कहा जाता है।
- गौरीशंकर डिजाइन – इसमें शिवलिंग के लिंग वाले हिस्से पर गौरी या महिला की मुखाकृति तराश दी जाती थी जिसकी वजह से इसे गौरीशंकर डिजाइन कहा जाता था।
पार्वती: आमतौर पर पार्वती की मूर्ति को प्रणाम मुद्रा में बनाया जाता था। इसमें दो अन्य डिजाइन भी मिलते हैं। एक, जिसमें मूर्ति के पीछे एक आधार बनाया जाता था जिसे बद्राधर या दीवालदार डिजाइन कहा जाता था। इसमें पार्वती को बैठी हुई मुद्रा में बनाया जाता था और मूर्ति को आधार पर उकेरा या तराशा जाता था। इसका एक दूसरा डिजाइन ट्यूशन क्लास में शुरू किया गया था जिसे निर्गम डिजाइन कहा गया। गया। इस डिजाइन की मूर्तियों के पीछे आधार नहीं होता था।
गणेश: इनकी मूर्ति अनेक स्वरूपों में आधार और आधार के बिना, दोनों ही तरीके से बनाई जाती थी। गणेश की मूर्तियों के दो स्वरूप प्रचलित थे। बैठे हुए गणेश और नृत्य करते गणेश। बैठे हुए गणेश की दो मुद्राएं थी, आसनधर औरआशीष मुद्रा। दोनों ही मुद्राओं में गणेश मुकुटधारी और जनेऊधारी होते थे। जनेऊ बायें कंधे से झूलते हुए कमर में दायीं तरफ जाता है। उनके चार हाथ होते थे। आमतौर पर बायीं हाथ में गंडासा (ऊपर) और मिठाई या लड्डू (नीचे वाली हाथ) बनाया जाता था। अपनी दायीं हाथ (ऊपर) में गणेश फरसा और नीचे वाली हाथ में माला पकड़े होते थे। सूंढ को सुविधानुसार बनाया जाता था, कभी सीधी कभी किसी भी दिशा में मुड़ी हुई। दोनों पैर आमतौर पर एक आधार पर गुणाकार बनाया जाता था। इस मुद्रा को आसनधर मुद्रा कहा जाता था। गणेश की मूर्ति आशीष मुद्रा में बनती थी जिसमें उनके दायें पैर का अंगूठा भूमि-स्पर्श मुद्रा की तरह दिखाया जाता था। गणेश की बॉम्बे कट मूर्ति भी बनती थी जिसमें उनकी सूंढ़ को बायीं तरफ मुड़ा दिखाया जाता था। कभी बॉम्बे (मुंबई) में ऐसी मूर्तियों की मांग अधिक थी। इसी वजह से उसे बॉम्बे कट कहा जाता था। गणेश के वाहन चूहे को अक्सर आधार में उभार दिया जाता था।
नंदी: बसहा या नंदी को शंकर का वाहन माना जाता है। नंदी को मुख्यरूप से दो डिजाइन में बनाया जाता है और दोनों ही मुद्रा में उसे बैठा हुआ बनाने की परंपरा रही है। उनमें एक डिजाइन का नाम कुकरू था जिसमें नंदी के चारों पैर बनाये जाते थे और दूसरा डिजाइन पसर था जिसमें केवल अगले दोनों पैरों को बनाया जाता था।
कृर्तमूर्त: यह कार्तिकेय या श्याम कार्तिक की मूर्ति होती थी। ये दो स्वरूप में बनाये जाते थे। पहले स्वरूप में कार्तिक को छह सिर और चार हाथ वाला बनाया जाता था जो मोर पर विराजमान रहते थे। उनके तीन हाथों में धनुष, माला और कमंडल दिखाया जाता था जबकि चौथा हाथ आमतौर पर खाली होता था। इस डिजाइन की मूर्ति मांग पर बनायी जाती थी। कार्तिकेय का दूसरा स्वरूप जिसे कृर्तमूर्त कहा जाता है, उसमें धड़ नहीं बनाया जाता था। ऐसी मान्यता है कि कार्तिकेय ने एक बार क्रोधवश अपने शरीर के सभी अंगों को खा लिया था। इसलिए इस स्वरूप में केवल उनका मुख बनाया जाता है। माना जाता है कि कृर्तमूर्त कीर्त मुख का अपभ्रंश है।
बुद्ध: इनकी प्रतिमाएं मुख्यत: तीन मुद्राओं में बनायी जाती थीं। पहली – भूमिस्पर्श मुद्रा, दूसरी – उपदेश मुद्रा और तीसरी अभयवर्धन मुद्रा। इन मूर्तियों को बद्राधर और निर्गम दोनों ही तरह का बनाया जाता था।
भूमिस्पर्श मुद्रा: इसमें बुद्ध ध्यान लगाए पद्मासन की मुद्रा में बैठे बनाये जाते हैं जिसमें उनका बायां हाथ अंक यानी जांघ पर और दाहिना हाथ आसन के नीचे पृत्वी की ओर संकेत करता दिखाया जाता था। बुद्ध के शरीर पर चादर या धोती भी उकेरा जाता था। मूर्ति बद्राधर डिजाइन में बनायी जाती थी जिसमें अनेक आलंकारिक तत्व शामिल किये जाते थे।
उपदेश मुद्रा: बुद्ध की मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में बनायी जाती थी जिसमें उनकी हाथ का भाव व्याख्यान मुद्रा में होता है और दाहिने हाथ का अंगूठा और कनिष्ठिका, बाएं हाथ की माध्यमिका को स्पर्श करती हुई दिखायी जाती है। इस डिजाइन को सारनाथ डिजाइन भी कहा जाता था। इसमें बुद्ध के मस्तक के पीछे एक प्रभामंडल भी बनाया जाता था।
अभयवर्धन मुद्रा: इस मुद्रा की मूर्तियों में बुद्ध को खड़ा बनाया जाता था वे दायें हाथ की हथेली को सामने की ओर खुली रखकर अभय वचन देते हुए दिखाये जाते थे।
खरल: यह दो डिजाइन में बनाया जाता था। एक नावनुमा जिसे किश्तीनुमा आकार कहा जाता है और दूसरा गोलाकर। किश्तीनुमा खरल आमतौर पर घरेलू उपयोग के काम आता था। खरल के साथ एक लोढ़ी रहती थी जो औषधियों के कूटने के काम आती थी। गोलाकर खरल का उत्पादन कम होता था क्योंकि इसकी मांग सीमित थी। साठ के दशक में इसका निर्माण सिर्फ भगवानदास गौड़ कर रहे थे। यह परंपरागत डिजाइन नहीं था। इसे वे लोग खरीदते थे जिन्हें मशीन के उपयोग से दवाओं का उत्पादन करना था। दो पाटों वाला खरल दवाओं को पीसने के काम आता था।
उत्पादन का समय
घरेलू उपयोग के उत्पादों और बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सालों भर किया जाता था क्योंकि इनकी मांग की कोई निश्चित अवधि नहीं थी और उनके विपणन में भी बहुत समस्याएं नहीं थी। कुछ प्रस्तर-उत्पादों को बनाने की प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू की जाती थी जिसमें पंचदेवता की मूर्तियां प्रमुख थीं। पंचदेवता एक ही फलक पर बनाने का रिवाज था और पंचदेवता को अगल-अलग भी बनाया जाता था जिनका संयोजन करके उन्हें स्थापित किया जाता था। उन्हें फाल्गुन या चैत में रामनवमी से पहले स्थापित करने की परंपरा थी। मंदिरों में भी पंचदेवता की मूर्तियों की स्थापना आमतौर पर जेठ माह में यानी मई-जून में की जाती थी। पत्थरकट्टी में भी आपको पंच देवता स्थापित मिल जाएंगे। महादेव की मूर्ति की मांग सालों भर थी जबकि कृष्ण की मूर्तियों की मांग जन्माष्टमी के समय और कार्तिक (अक्टूबर-नवंबर) के महीने में काली की मूर्तियों की मांग
बढ़ जाती थी।
कच्चा माल
घरेलू उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन हो या मूर्तियों का निर्माण, इसकी प्राथमिक शर्त्त थी अलग-अलग प्रकार के पत्थरों की उपलब्धता। 1970-80 के दशक तक ज्यादातर पत्थर स्थानीय खदानों में उपलब्ध थे। घरेलू उपयोग की वस्तुओं में खरल और कुंडी प्रमुख थे जिन्हें पीरकसौटी, पराजित या धनमहुआ और मोतिया पत्थर से बनाया जाता था। पीरकसौटी और पराजित मुलायम पत्थर हैं और उन्हें मनचाहा आकार देना ज्यादा आसान था। छोटे खरल (दो इंच से 12 इंच) इन्हीं पत्थरों से बनाए जाते थे। मोतिया पत्थर अपेक्षाकृत कड़ा पत्थर है और आमतौर पर उससे मध्यम आकार के खरल बनाये जाते थे (छह इंच से चौबीस इंच)। इनके अलावा स्थानीय तामरा और हंसराज पत्थर का प्रयोग भी खरल बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इनसे बड़े खरल बनाये जाते थे जिनका उपयोग आयुर्वेदिक दवा कंपनियां करती थी। यह मोतिया से भी कड़ा पत्थर था। कुंडी बनाने के लिए आमतौर पर पराजित पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह पीरकसौटी से सस्ता उपलब्ध था। इसके लिए सिंहभूम, सरायकेला और घाटशिला के पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था।
आनुष्ठानिक मूर्तियों के निर्माण में, खासतौर पर पंचदेवता बनाने के लिए पराजित पत्थर का उपयोग किया जाता था। इसे सिंहभूम पत्थरों से भी बनाया जाता था। आनुष्ठानिक मूर्तियां का प्रयोग सजावट के लिए भी किया जाता था, इसी वजह से भी उन्हें पराजित और पीरकसौटी पत्थर से बनाया जाता था। इन पत्थरों में उन्हें मनचाहा आकार देना संभव था। मूर्तियों में चिकनापन लाने और उन पर बारीक लाइनों को उकेरने के लिहाज से भी ये उपयुक्त पत्थर थे। बुद्ध, शिव, सरस्वती, काली और सूर्य की प्रतिमाओं को बनाने में इन्हीं पत्थरों को प्रयोग किया जाता था। इन दोनों पत्थरों की एक खासियत यह भी थी कि मूर्तियों को रंगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मोम या तेल मलने से उनका रंग काला हो जाता था।
पत्थरों के स्रोत
पत्थरकट्टी में स्थानीय स्तर पर ही अनेक प्रकार के पत्थर उपलब्ध थे। पीरकसौटी पत्थर पत्थरकट्टी पहाड़ की खदानों से आता था। इस पत्थर की खदान के पास एक पीर का मजार था जिसकी वजह से इसे पीरकसौटी कहा जाता था। मोतिया पत्थर भी पत्थरकट्टी पहाड़ में उपलब्ध था। इन पत्थरों में छोटे-छोटे सफेद धब्बे होते की वजह से उन्हें मोतिया पत्थर कहा जाता था। पराजित या धनमहुआ पत्थर धनमहुआ पहाड़ से आता था जिसे कटारी पहाड़ भी कहा जाता है।
तामरा पत्थर पत्थरकट्टी और कटारी पहाड़ दोनों ही जगहों पर उपलब्ध था। इस पत्थर में तांबे के निशान मिलते हैं जिसकी वजह से इसे तामरा पत्थर कहा गया। इससे बने उत्पाद दीर्घकाल तक चलते हैं और अन्य पत्थरों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते थे। हंसराज पत्थर भी पास ही में उपलब्ध था।
मूर्तियों के तराशने के बाद उन्हें परिष्कृत करने के लिए तीन अलग-अलग पत्थरों से उनकी घिसाई की जाती है। हालांकि 70 के दशक तक कार्बोरंडम पत्थर का प्रयोग भी शुरू हो गया था। घिसाई के बाद मूर्तियों को रंगा जाता है या मोम या तेल मलकर उन्हें काला किया जाता है। ये सारी चीजें स्थानीय बाजार में उपलब्ध थीं।
1970-80 के दशक में पत्थरकट्टी के खदानों पर परिवारों की दावेदारी मिलती है। दरअसल 1950 में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् पहाड़ सरकार के अधीन हो गये थे। तब सरकार ने नियम और शर्तों के साथ खादानों को पाषाण-शिल्पियों के हवाले कर दिये ताकि वे पाषाण-शिल्प जारी रखें और बदले में सरकार को रॉयल्टी देते रहें। इस पद्धति में कोई लिखत-पढ़त नहीं होती थी। 1961 की जनगणना रिपोर्ट में खादान और संबंधित शिल्पकारों की चर्चा इस प्रकार की गयी है –
| खदान | स्वामित्व |
| पीर कसौटी खदान – 1 | रामनाथ गौड़, शिबरथ गौड़, माधव गौड़, गंगा प्रसाद गौड़, छोटू लाल गौड़, राम निवास गौड़ा |
| पीर कसौटी खदान – 2 | तुलसीराम गौड़, धन्नालाल गौड़, हीरालाल गौड़, छोटा रामनाथ गौड़, रामप्रसाद गौड़, भुवनलाल गौड़, रामधनी गौड़, राजालाल गौड़, हरिप्रसाद गौड़, मोतीलाल गौड़ |
| मोतिया – 1 | सहयोग समिति |
| मोतिया – 2 | हीरालाल गौड़, धन्नालाल गौड़ |
| तामरा | सभी के लिए |
| हंसराज | सभी के लिए |
| पराजित – 1 | छोटा हीरालाल गौड़, शिवनारायण गौड़, धन्नालाल गौड़ (छोटे), तुलसीराम गौड़, रामप्रसाद गौड़ |
| पराजित – 2 | हीरालाल गौड़, बड़ा धन्नालाल गौड़ और उसके तीन भाई |
| पराजित – 3 | रामप्रसाद गौड़ |
| पराजित – 4 | भुवनलाल गौड़, मदनलाल गौड़, रामनाथ गौड़, शिबरथ गौड़, माधवलाल गौड़ |
| पराजित – 5 | सभी के लिए |
उपकरण और औजार
पत्थरों को तोड़ने के लिए मुख्य रूप से लोहे के घन या हथौड़े का उपयोग किया जाता था और मूर्तियों को आकार देने के लिए हथौड़ी का। हथौड़ी घन से छोटी होती है। दोनों ही कामों में अलग-अलग तरह की छेनी का प्रयोग किया जाता था। इस तरह से हथौड़ा, हथौड़ी और छेनी पाषाण शिल्प के मुख्य उपकरण और औजार थे। पाषाण शिल्पियों के सभी परिवारों में ये उपकरण आज भी मिल जाएंगे। इन्हें स्थानीय लोहार से खरीदा जाता था। ये खुखरी-नियामतपुर और गया से खरीदे जाते थे। उपयोग के आधार पर छेनी के अलग-अलग रूप होते थे जिन्हें तकला, तकली या चिरनी कहा जाता था। तकला से पत्थर को शुरुआती आकार दिया जाता था जबकि तकली से उस आकार को परिष्कृत किया जाता था। इसका उपयोग मूर्तियों पर उत्कीर्णन या बारीक कारीगरी के लिए भी किया जाता था। चिरनी का प्रयोग मुख्य रूप से मूर्तियों की सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता था। पत्थरों पर लाइन खीचने और उत्पादों की मोटाई मापने के लिए प्रकाल का प्रयोग किया जाता था। वैसे माप लेने के लिए लोहे के स्केल का सहारा लिया जाता था जिसे गुनिया कहते थे।
खदान से पत्थरों को निकालने के लिए रम्भा, गोदाल या खंती का प्रयोग किया जाता था। यह लोहे की मोटी छड़ होती थी जिसका एक सिरा चपटा होता था। यह चट्टानों में छेद करने के काम भी आता था ताकि विस्फोट के जरिए चट्टानों को तोड़ा जा सके। अब वहां विस्फोटकों से चट्टान तोड़ने की मनाही है। बड़ी चट्टानों में छेद करने और उनके टुकड़े करने के लिए खंती और लोहे की गुली का प्रयोग किया जाता था। उपकरणों को धारदार बनाने के लिए रेंती का प्रयोग किया जाता था।
प्रस्तर मूर्तियों और उत्पादों के डिजाइन, संबंधित पत्थरों और उनके स्रोत, उपकरणों, खदानों पर अधिकार आदि की चर्चा 1961 की जनगणना रिपोर्ट में की गयी है। हालांकि अब खदानों पर परिवारों का अधिकार नहीं रहा और अधिकतर खदानें बंद हो गयी हैं। यहां तक कि स्थानीय स्तर पर पत्थर नहीं के बराबर उपलब्ध हैं। इस स्थिति में शिल्पियों को पत्थर जयपुर, मकराना, दुमका, चुनार, झांसी आदि स्थानों से लाना पड़ता है। शिल्पियों के ज्यादातर औजार आज भी परंपरागत हैं, हालांकि अब छोटे-छोटे इलेक्ट्रिक कटर का प्रयोग किया जाने लगा है। इतना ही नहीं, आज भी शिल्प-उत्पादों के डिजाइन न केवल परंपरागत हैं बल्कि वे पहले के मुकाबले तकनीकी स्तर पर कम परिष्कृत दिखते हैं।
—
References:
Personal interview with Ravindranath Gaur, Sunil Kumar, 2018, Patharkatti, Gaya.
Need Assessment Survey Report, MSME Design Clinic Scheme, 2013, Upendra Maharathi Shilp Anusandhan Sansthan, Patna.
Census of India, 1961, Volume IV, Bihar, Craft Survey Report: Stoneware Craft of Patharkatti Village (District Gaya)
Personal interview with sculptors – Ravindranath Gaur, Sureshlal Gaur, Amarnath Gaur
Other links:
Photo Documentation: Patharkatti, Village of Stone Carvers, Gaya, Bihar
पत्थरकट्टी,1940–1970: परंपरा और परिस्थितियों के बीच फंसा पाषाण शिल्प
पाषाण शिल्पियों का विशिष्ट गांव, पत्थरकट्टी: संक्षिप्त इतिहास और सामाजिक तानाबाना
–
Tags: craft village, Crafts village history, Gaur brahmins, Patharkatti, Ravindranath Gaur, Stone carving